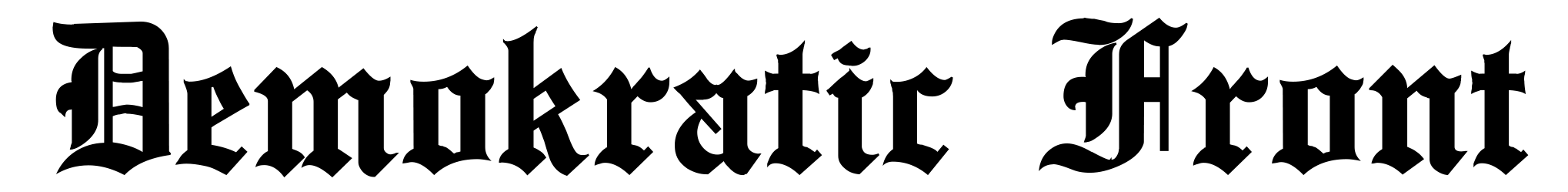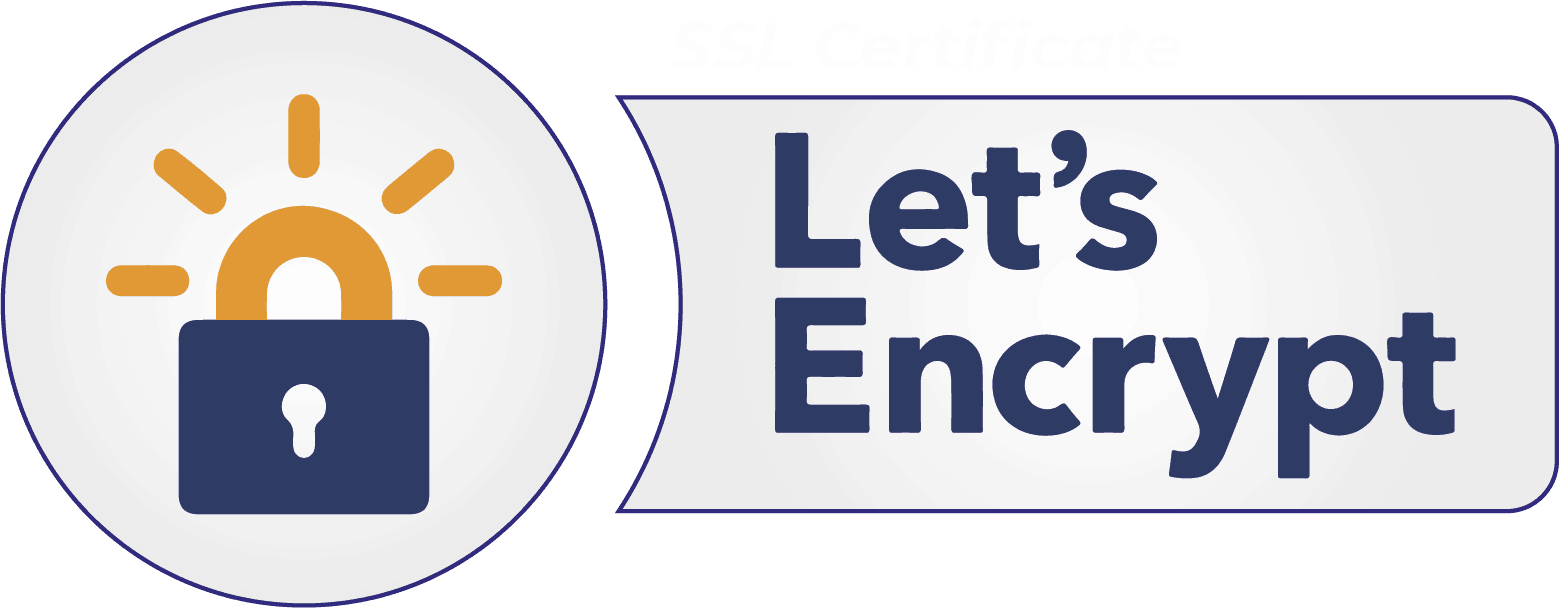Despite the recurring strife in bilateral ties, India and Pakistan continue to work together on humanitarian issues. Official sources…
Month: June 2018
एजेंसियों को दो अरब डॉलर की कथित पीएनबी धोखाधड़ी के मामले में फरार नीरव मोदी के पास कम से…
A US association of immigration advocates recently filed a lawsuit against the United States Citizenship and Immigration services(USCIS), seeking…
रोहतक 17 जून : आज महम में आयोजित कार्यकर्त्ता सभा में मौजूद भारी संख्या में कार्यकरताओ से आर-पार की…
अलग पंजाबी राष्ट्र बनाने के अलगाववादी रेफरेंडम-2020 का समर्थन करने पर आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा चौतरफा हमलों में…
हालांकि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा संविधान में किया गया है। इसे दस साल में पूरा करने का लक्ष्य…
अपने गोलकीपर कैस्पर इश्माइकल की बेहतरीन गोलकीपिंग और यूसुफ पाउलसन युरारी द्वारा 59वें मिनट में गिए गए गोल के दम…
आठ साल बाद विश्व कप में कदम रख रही सर्बिया की टीम ने कप्तान एलेक्जेंडर कोलारोव द्वारा फ्रीकिक पर…
अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप में आइसलैंड के खिलाफ खेले गए मैच के दूसरे हाफ…
जम्मू एंड कश्मीर में सेना के जवान औरंगजेब की शहादत के बाद हालात काफी अलग हैं. इस घटना के बाद…